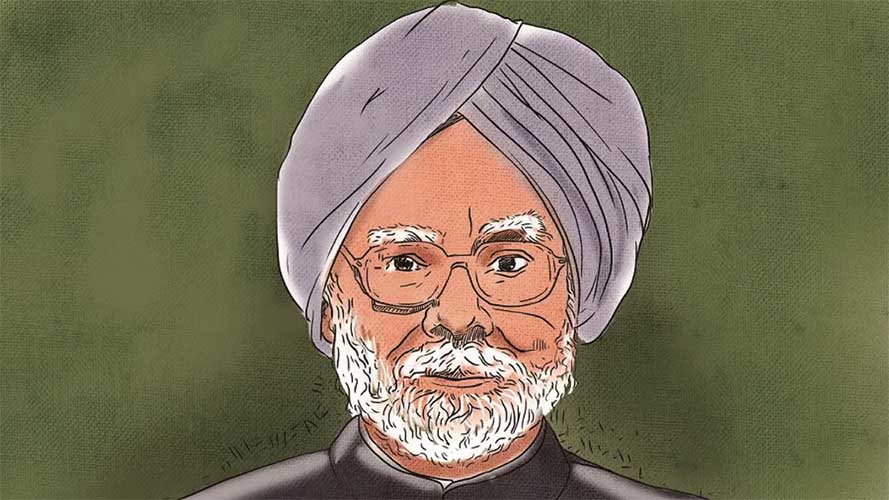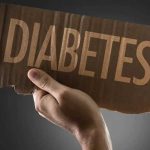हमारा संबंध अनोखा था या कह सकते हैं विचित्र भी। भारत के अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया, बाजार अर्थशास्त्र के पारंपरिक ताने-बाने से जुड़े हुए थे। वहीं दूसरी ओर अनिल अग्रवाल एक कट्टर पर्यावरणविद् थे। 1991 में, जब मनमोहन सिंह भारत को विनियमन मुक्त और व्यापार के लिए सीमारहित, उदारवादी दुनिया में लेकर आए, तब हम उनके समर्थकों में शामिल नहीं थे।
हमारे लिए, मुद्दा यह था कि उदारीकरण के पर्यावरण के लिए क्या मायने होंगे। हमारी नियामक संस्थाएं कमजोर थीं और इसलिए अर्थव्यवस्था के खुलने से प्रदूषण और क्षरण होना लाजमी था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि मनमोहन सिंह ने हमें खारिज नहीं किया और यही बात उन्हें अपने क्षेत्र के अन्य लोगों से अलग बनाती थी। उन्होंने हमसे बातचीत की। इसका मतलब यह नहीं है कि उन्होंने हमारी बात मान ली। लेकिन वह समझते थे कि यह एक ऐसी दुनिया थी जिसके बारे में उन्होंने सोचा नहीं था। वह इसके बारे में और जानना चाहते थे; वे यह समझना चाहते थे कि संतुलन पाने की दिशा में सिस्टम को मजबूत करने के लिए क्या किया जा सकता है। “संतुलन” ही उनके लिए मुख्य शब्द था।
1990 के दशक के मध्य में जब अनिल ने उद्योग जगत के लिए पहला पर्यावरण-रेटिंग कार्यक्रम शुरू किया, तब सिंह सलाहकार समिति की अध्यक्षता करने के लिए सहमत हुए। हमारा प्रयास न केवल प्रदर्शन को बेंचमार्क करने के लिए था, बल्कि व्यवसायों को आगे बढ़ाने और प्रोत्साहित करने के लिए मापने वाले संकेतकों का उपयोग करने के लिए भी था। उन्होंने उद्योग जगत से केवल विनियामक मानकों को पूरा करने से अधिक की मांग करने के हमारे प्रयास पर कोई संशय या हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उन्होंने भारत जैसे देश में परिवर्तनकारी कार्रवाई की आवश्यकता को समझा, जहाँ आर्थिक विकास के लिए आवश्यक प्राकृतिक संसाधन दुर्लभ हैं और प्रदूषण की वजह से चीजों की लागत बढ़ जाती है, जिसे गरीब वहन नहीं कर सकते।
2004 में जब सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने तब तक अनिल का निधन हो गया था और मैं सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट का नेतृत्व कर रही थी। मैं उम्र में छोटी होने के साथ-साथ बहुत कम अनुभवी थी, लेकिन एक बार भी सिंह ने मुझे अपर्याप्त महसूस नहीं कराया। मैं प्रधानमंत्री कार्यालय में उनसे मिलने जा सकती थी। वे जल संरक्षण से लेकर जलवायु परिवर्तन तक के मुद्दों पर मेरे विचार जानना चाहते थे । उन्होंने न केवल मेरी बात सुनी, बल्कि मुझे समाधान प्रदान करने के लिए प्रेरित किया। “क्या किया जाना चाहिए”, यह उनका लक्ष्य था।
2005 में उन्होंने मुझे बाघ संरक्षण की समीक्षा करने वाली समिति की अध्यक्षता करने के लिए कहा। मैं उनके मुझ पर विश्वास से अभिभूत थी। यह देखते हुए कि समिति के अन्य सदस्य इस क्षेत्र के दिग्गज थे या देश की शक्तिशाली संरक्षण लॉबी से जुड़े थे। यह एक कठिन समय भी था। एक तरफ, भारत ने सरिस्का बाघ अभयारण्य में सभी बाघों को खो दिया था।
दूसरी ओर यह वह समय भी था जब वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) पर चर्चा हो रही थी, ताकि आदिवासियों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय की क्षतिपूर्ति करने के लिए उन्हें उस भूमि पर स्वामित्व मिले, जिस पर वे रहते हैं। लेकिन वह वनभूमि थी और कुछ मामलों में, राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के अंतर्गत थी जहां बाघ और अन्य जानवर पाए जाते थे। यहां एजेंडे का टकराव होने के साथ-साथ एक वर्ग युद्ध भी था, संरक्षण बनाम आदिवासी।
सिंह स्पष्ट रूप से बीच में फंस गए थे। वह दोनों पक्षों का सम्मान करते थे और एक को छोड़कर दूसरे को चुनना नहीं चाहते थे। दोनों हितों का संतुलन ही वह चीज थी, जिसकी उन्होंने तलाश की।
मैंने आधिकारिक प्रस्तुति से कुछ दिन पहले उन्हें रिपोर्ट दिखाई। मैं चाहती थी कि वे कार्रवाई के एजेंडे को समझें, विशेष रूप से संरक्षण के समावेशी प्रतिमान की आवश्यकता को। उन्होंने पक्ष और विपक्ष को समझा और पूछा कि क्या मुझे यकीन था कि यह संभव है और क्या प्रमुख हितधारक इसमें शामिल हैं?
मैंने उनसे कहा कि यह मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है। मेरा अनुरोध था कि रिपोर्ट ‘जॉइनिंग द डॉट्स’ को सार्वजनिक किया जाना चाहिए] क्योंकि इससे एजेंडे के बारे में जागरूकता पैदा होगी और नीति परिवर्तन को बढ़ावा मिलेगा। मेरा डर था कि इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा।
जैसा कि अक्सर कई रिपोर्टों का हश्र होता है। यहां श्री सिंह की तारीफ करनी होगी। बाघों के संरक्षण के क्षेत्र में बहुत कार्रवाई हुई। उनकी संख्या बढ़ी है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे पास गिनती के बेहतर तरीके हैं ताकि यह पैरों के निशान नहीं बल्कि बाघों की गिनती हो।
बाद में उन्होंने मुझे जलवायु परिवर्तन और गंगा की सफाई के लिए बनी प्रधानमंत्री की परिषद का सदस्य बनाया। किसी मामले में मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे अपने विचार व्यक्त नहीं करने चाहिए] चाहे वे कमरे में मौजूद अन्य लोगों से कितने ही भिन्न क्यों न हों। वास्तव में मेरे रुख को (हमेशा की तरह, हमारी सोच की सीमा को आगे बढ़ाने के लिए) उन्होंने प्रोत्साहित किया] लेकिन इस चेतावनी के साथ कि समाधान व्यवहार्य होना चाहिए।
यही कारण है कि सिंह और उनकी राजनीति एवं व्यक्तित्व का खास ब्रांड हमारी चरमपंथी दुनिया में याद किया जाएगा। आज हम बुलबुले में रहते हैं जहां हम केवल उन लोगों की राय पढ़ते और सुनते हैं जिनसे हम सहमत हैं। हमारे पास दूसरे के विचारों के लिए समय नहीं है या क्योंकि यह उन फार्मूलों में फिट नहीं बैठता है जो आमतौर पर स्थापित नियमों की टेक्स्टबुक में कारगर माने जाते हैं।
उनके अपने स्वयं के विचार भी थे, चाहे वे अनुभव जनित हों या टेक्स्टबुक वाले। लेकिन उन्होंने कई दरवाजे खोले क्योंकि उनके विचारों में खुलापन था जो बदलाव के प्रति उनकी प्रतिबद्धता से प्रेरित था।
वह एक सौम्य दिग्गज थे जिन्होंने सत्ता को बेहतर बनाया। यह हमारी स्थिति के अनुरूप नहीं है और इसलिए अप्रासंगिक हैं। क्योंकि यह उन कार्यों के सूत्र में फिट नहीं बैठता है जिनके बारे में हमें सिखाया गया है और उनके कारगर होने का भरोसा हो, नियमों की स्थापित पुस्तक।
सिंह के पास पहले से प्रस्तावित विचार भी थे। चाहे पाठ्यपुस्तक में क्या था या उनका अपना अनुभव हो। लेकिन उन्होंने दरवाजे खोले क्योंकि उनके पास विचारों का खुलापन था, जो बदलाव के प्रति उनकी प्रतिबद्धता से प्रेरित था। वह एक सौम्य दिग्गज थे जिन्होंने सत्ता को बेहतर बनाया।

आलेख: सुनीता नारायण (साभार: डाउन टू अर्थ)